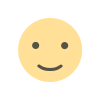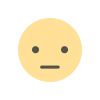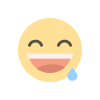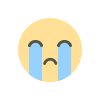नज़्म

कैफ़ी आज़मी
रोज़ बढ़ता हूँ जहाँ से आगे
फिर वहीं लौट के आ जाता हूँ
बार-हा तोड़ चुका हूँ जिन को
उन्हीं दीवारों से टकराता हूँ
रोज़ बसते हैं कई शहर नए
रोज़ धरती में समा जाते हैं
ज़लज़लों में थी ज़रा सी गर्मी
वो भी अब रोज़ ही आ जाते हैं
जिस्म से रूह तलक रेत ही रेत
न कहीं धूप न साया न सराब
कितने अरमान हैं किस सहरा में
कौन रखता है मज़ारों का हिसाब
नब्ज़ बुझती भी भड़कती भी है
दिल का मामूल है घबराना भी
रात अन्धेरे ने अन्धेरे से कहा
एक आदत है जिए जाना भी
क़ौस इक रंग की होती है
तुलू एक ही चाल भी पैमाने की
गोशे-गोशे में खड़ी है मस्जिद
शक्ल क्या हो गई मय-ख़ाने की
कोई कहता था समुन्दर हूँ मैं
और मिरी जेब में क़तरा भी नहीं
ख़ैरियत अपनी लिखा करता हूँ
अब तो तक़दीर में ख़तरा भी नहीं
अपने हाथों को पढ़ा करता हूँ
कभी क़ुरआँ कभी गीता की तरह
चन्द रेखाओं में सीमाओं में
ज़िन्दगी क़ैद है सीता की तरह
राम कब लौटेंगे मालूम नहीं
काश रावण ही कोई आ जाता
आपकी प्रतिक्रिया क्या है?